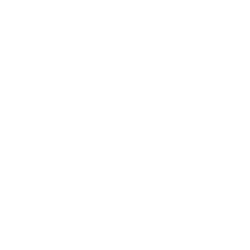
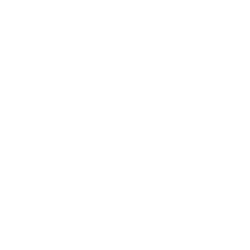

" विद्वान सर्वत्र पूज्यते " इस उक्ति के अनुसार धारानगरी के मुंजराजा और भोजराजा ने कवीश्वर धनपाल की विद्वता और सर्जनकला से प्रसन्न होकर उन्हें सदैव आदर दिया था । मुंजराजा उन्हें पुत्र के समान मानते थे और उनकी विद्वता देखकर उन्हें " कूर्चाल सरस्वती " ( दाढ़ी -मूँछवाली विद्यादेवी सरस्वती ) का बिरुद दिया था । भोजराजा ने अपने हितैषी और राज्य के परम विद्वान कवि धनपाल को " कवीश्वर " एवं " सिद्ध सारस्वत " ऐसें दों बिरुदों से अलंकृत किये थे ।
एक समय पर कवि धनपाल ने जैन धर्म के प्रति द्वेष के कारण मालवा में जैन साधुओं के विहार पर राजा द्वारा प्रतिबंध घोषित करवाया था । दूसरी ओर उसके छोटे भाई शोभन तो जैन साधु का महिमापूर्ण जीवन पसंद करके शोभनाचार्य बने थे । उन्होंने अपने बड़े भाई को को जैनदर्शन की महत्ता और व्यापकता का स्मरण करवाया , इसलिए कविश्वर सच्चे हृदय से वीतराग देव की भक्ति करने लगे । कवि धनपाल ने नव-रसों से परिपूर्ण बारह हजार प्रमाणसभर तीर्थकर श्री ऋषभदेव भगवान की स्तुतिप्रधान मनोहर गद्यकथा की रचना की । इसके लिए गुजरात में विचरण करते हुए आचार्यश्री शांतिसूरीश्वरजी की धारानगरी में महोत्सवपूर्वक पधरावनी करवाई थी । आचार्यश्री के पास इस कथा का संशोधन करवाया । आचार्यश्री ने कई वादियों को जीते होने से उन्हें धारानगरी के राजा भोज द्वारा " वादिवैताल " का सम्मानीय बिरुद प्राप्त हुआ ।
एक समय जाड़े की रात में कवि ने अपनी भावपरिपूर्ण वाणी में राजा भोज को लालित्यसभर यह कृति सुनाई , तब राजा ने कहा कि , इसमें वह परिवर्तन करके उनके धर्म तथा उनकी प्रशंसा के शब्द रखेंगे तो कवि जो माँगेंगे वह देंगे । कविराज धनपाल ने राजा भोज से कहा , " ऐसा परिवर्तन करना यह तो अपने हृदय की भावधारा का द्रोह करने के समान माना जाय , अतः मुझे क्षमा कीजिये । "
कवि के स्पष्ट कथन से राजा भोज में क्रोध का दावानल भड़क उठा । इस गद्य-कथा का ग्रंथ राजा ने निकट रखी अँगीठी में डालकर जला दिया । उसके बाद कवि और राजा के बीच काफी कहा -सुनी हुई ।
भारी हृदय से कवि धनपाल घर आये । उनकी आँखों में दुःख था । चेहरे पर व्यथा थी । हृदय में बैचेनी थी । उनकी पुत्री तिलकमंजरी पिता का दुःख परख गई । उसके पिता को ऐसी उदासीनता का कारण पूछा ।
तिलकमंजरी कवि धनपाल की प्राणप्रिय बेटी थी । पिता ने अपनी विद्या का उसे उतराधिकार दिया था । छोटी आयु की होते हुए भी वह विदुषी थी । पिता धर्मभक्ति के भाव में डूबकर तथा वीतरागप्रिती में एकरुप होकर जिस भक्ति से गद्य -कथा का सर्जन करते थे , उसका तिलकमंजरी रोज पठन करती थी । इस प्रभु कथा में उसे इतना अधिक रस प्राप्त हुआ कि उसने उसके एक-एक शब्द को अपनी स्मृति में संभालकर रख छोड़ा था । कवीश्वर धनपाल ने वेदनामय निश्वास डालते हुए यों कहा कि वर्षो की उनकी साहित्यसाधना को राजा ने अपने गुस्सें में पलभर में भस्म कर डाला ।
तिलकमंजरी ने कहा , " पिताजी , आप तनिक भी व्यग्र न हों । राजा ने भले ही उस ग्रंथ के पृष्ठों को जला डाला हों , परंतु उस ग्रंथ का साहित्यरस तो मेंरे चित्त में सुरक्षित हैं , संपूर्ण ग्रंथ मुझे याद हैं । "
कवि के आनंद की सीमा न रही । अपनी पुत्री के लिए उन्हें गर्व हुआ । उसकी स्मरणशक्ति के लिए मान हुआ । स्वयं दिये हुए साहित्य के संस्कार कठिन समय में कितने अधिक लाभकर्ता सिद्ध हुए इसका विचार कवि धनपाल करने लगे । तिलकमंजरी के मुख से गद्यकथा प्रवाहित होने लगी और कवि धनपाल उसे लिखने लगे । कुछ भाग तिलकमंजरी ने सुना या पढ़ा नहीं था , उतना ही भाग कृति में अधूरा रह गया । कवि धनपाल ने उस बाकी भाग की रचना करके कथा को अखंड स्वरुप दिया ।
विक्रम संवत् 1084 में यह घटना घटी । नव या नौ रसों से भरपूर उत्कृष्ट गद्यकथा की रचना हो गई । कवीश्वर धनपाल को अपने जीवन की सार्थकता का अनुभव हुआ । ऐसी बेटी प्राप्त नहीं हुई होती तो अपनी गद्यकृति का कौन जाने क्या होता ? इसलिए कविश्वर धनपाल ने इस कृति का नाम " तिलकमंजरी " रखा । धन्य है तिलकमंजरी की उस स्मरणशक्ति को कि जिसने एक महान ग्रंथ को पुनः सर्जन-आकाररुप दिया ।
साभार : जिनशासन की कीर्तिगाथा